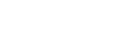कामकाजी मांओं के लिए 2-4 या 10-12 दिनों के लिए काम के खातिर शहर से बाहर जाना एक पूरा चैलेंज होता है. जो परिवार घर की महिला को तीर्थयात्रा के नाम पर 10-12 दिनों के लिए सहर्ष भेज देने को तैयार रहते हैं, वे उसे काम के सिलसिले में अकेले भेजने से कतराते हैं. यह एक तरह की सामूहिक गुलामी का परिणाम है, जिस का शिकार बहुत से समाज हैं और भारतीय समाज तो बहुत ही ज्यादा है.
हमारे यहां समझा जाता है कि अकेली जाने वाली महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है न बस में, न ट्रेन में और न ही हवाईजहाज में. जब तक बहुत अनुभवी न हों, ज्यादातर अकेली औरतें वास्तव में भयभीत हिरणी की तरह दिखती हैं, जिसे मानो भेडि़यों के झुंड में छोड़ दिया गया हो.
यह सामाजिक अंकुश असल में समाज ने औरतों के पर काटने के लिए लगाया है ताकि उन्हें जैसे चाहे घरों में रखा जाए और वे अकेले भाग कर मायके या रिश्तेदारों के यहां न जाएं. जहां पुरुष ‘दौरे पर जा रहा हूं’ कह कर 5-7 दिन कहां जा रहा है और कहां ठहरेगा जैसे सवालों के बिना भी जासकता है, वहीं लड़कियां या औरतें नहीं जा सकतीं.
यह बदला जाना चाहिए और घर में सुरक्षा के अधिकार के साथ ही घर से बाहर जाने का अधिकार भी संवैधानिक मानवीय अधिकारों में शामिल होना चाहिए.
पहले इस तरह का व्यवहार गुलामों के साथ किया जाता था. उन्हें मनमरजी से जाने का हक नहीं था. अगर अमेरिका में कोई अश्वेत सड़क पर चलता दिखता
था तो उसे पकड़ लिया जाता था. यही हाल औरतों के साथ भी होता है. उन्हें आज के कानून के और बराबरी के हक के राज में भी ऐसी संपत्ति मान लिया जाता है, जिसे जब मरजी उठवाया जा सके.