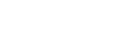तब मेरी उम्र कोई सात-आठ साल की रही होगी, जब मेरी परदादी जिन्दा थीं. लखनऊ में हमारा घर काफी बड़ा था. दरअसल यह पुराने वक्त की बनी एक कोठी थी, जिसमें ड्रौइंग रूम, डायनिंग रूम, बेडरूम, आंगन, रसोईघर, बाथरुम सब अलग-अलग बने हुए थे. आज भी बनारस, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद में ऐसी पुरानी कोठियां मौजूद हैं, जहां ऐसे पुराने आर्किटेक्चर दिखते हैं, जिसमें बड़े से आंगन के चारों ओर कमरे बने होते हैं. मेरी मां का ज्यादातर वक्त रसोईघर में बीतता था, जो बड़े से आंगन के उस पार बना था. आंगन के इस पार सबके सोने के कमरे बने थे. रसोईघर का एक दरवाजा आंगन की ओर और दूसरा अनाज के गोदाम में खुलता था.
इस रसाईघर में मां घर के पुराने नौकर की मदद से सबके लिए खाना तैयार करती थीं. नौकर उस खाने को डायनिंगरूम में लाकर टेबल पर सजाता था. फिर सब लोग वहां बैठ कर खाना खाते थे. खाने के वक्त भी मां डायनिंग टेबल पर नहीं होती थीं. वह उस वक्त भी रसोईघर में ही काम में जुटी रहती थीं. रोटियां-पूड़ियां तलती-बनाती, गर्म-गर्म निकाल कर डाइनिंग रूम में भिजवातीं. नौकर रसोईघर और डायनिंग रूम के बीच भाग-भाग कर डोंगे में खाना भर-भर कर पहुंचाता था. जब सब लोग खा लेते थे, तब सबसे अन्त में मां के खाने का नम्बर आता था, और वह रसोईघर में ही अपनी थाली लेकर बैठ जाती थीं.
उनका साथ अगर कोई देता था तो वह थीं मेरी परदादी, जो 85 साल की उम्र में भी लाठी टेकती आंगन पार करके मेरी मां के पास रसोइघर में जाकर बैठ जातीं और वहां मां के साथ ही खाना खाती थीं. मैंने कभी अपनी मां और परदादी को हमारे साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाते नहीं देखा था. उनकी जिन्दगी जैसे रसोईघर की चारदीवारी में ही सिमट कर रह गयी थी.