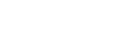जब मेरे पापा की मृत्यु हुई, पडोसी, रिश्तेदार, पंडितों का ज्ञान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, खूब पूजा पाठ, दान दक्षिणा की बात की जा रही थी, पापा टीचर थे, कई दिनों की बीमारी को झेल रहे थे, एम्स में उनका इलाज चलता रहा था, वहीँ लम्बे समय से एडमिट थे, मुज़फ्फरनगर से दिल्ली आने जाने में मम्मी और हम तीन भाई बहन काफी चक्कर लगा रहे थे, अब उनके जाने के बाद मम्मी के सामने और भी जरुरी चीजें थीं पर जैसा कि हमारे समाज में होता है कि जो धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया है, वही सच है, आम इंसान अपना आगे का जीवन कैसे जियेगा, इसकी चिंता धर्म के नियम बनाने वालों को कम रही है, खैर, मम्मी भी चूँकि टीचर थीं, तो उन्होंने अच्छी तरह से सोचा समझा और साफ़ कहा कि मैं किसी भी धार्मिक रीति में वो गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च नहीं करुँगी जो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा है, वो बचा हुआ पैसा मैं इन ढकोसलों में नहीं उड़ाऊँगी, सबका मुँह बन गया कि पढ़ लिख कर ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है, अब अपने मन की करेंगीं! अति आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए, पर मम्मी के साथ सबका व्यवहार ऐसा था कि पता नहीं मम्मी ने कितना बुरा काम कर दिया है जो वे रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पंडितों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुईं, काफी लम्बे समय तक वे लोगों की नाराजगियाँ झेलती रहीं. पद्रह दिन बाद जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो पड़ोस की कुछ महिलाएं उनके स्कूल निकलने के समय गेट पर आ गयीं और कहने लगीं, ''कम से कम एक महीना तो शोक मना लेतीं, आप तो बड़ी जल्दी तैयार होकर चल दीं. ''