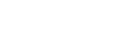साधुसंतों का रहनसहन और खानपान तो आम लोगों से भिन्न रहता ही है मगर वे मरने के बाद भी विशिष्ट दिखना चाहते हैं. इस के पीछे उन की व उन के संप्रदायों की मंशा महज धर्म के नाम पर चल रही दुकानदारी को और चमकाना होती है. धर्म के धंधे की बुनियाद ही यह है कि धर्म के रखवाले कहे जाने वाले साधुसंत ही हकीकत में धर्म के नाम पर लोगोें का तरहतरह से शोषण करते हैं, व्यवस्थित और संगठित समाज से अलगथलग दिखना चाहते हैं. महज लंगोट और गेरुए वस्त्र पहन सांसारिकता त्यागने का ढिंढोरा पीटने वाले साधुसंत शरीर पर भभूत और माथे पर बड़ा सा तिलक जरूर लगाते हैं. ये लोग हाथ में भाला, डंडा या त्रिशूल भी रखते हैं. यह ‘त्याग’ भक्तों में श्रद्धा पैदा करने के लिए किया जाता है. यह दीगर बात है कि हकीकत में यह हुलिया मुफ्त कमानेखाने यानी चढ़ावा और दक्षिणा हथियाने के लिए रखा जाता है.
अपनी सहूलियत के लिए साधुसंत रिहायशी इलाकों से कुछ दूर मंदिरों में रहते हैं. हाथ में पकड़ा डंडा या त्रिशूल दरअसल, दुष्टों के संहार के लिए नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्लियों और दूसरे जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखा जाता है. इस से सहज ही समझा जा सकता है कि भगवान के ये तथाकथित दूत और धर्मरक्षक असल में कितने चमत्कारी होते होंगे. बीते 2 दशकों से साधुसंतों में विचित्र तरह की एकजुटता देखने में आ रही है कि ये लोग भी साथसाथ रहने लगे हैं. ऐसा पहले की तरह शैव, वैष्णव या किसी दूसरे संप्रदाय की विचारधारा के अनुयायी होने न होने के कारण नहीं हो रहा बल्कि मुफ्त की रोटी तोड़ने तथा एक और एक ग्यारह बनने का सिद्धांत इस के पीछे काम कर रहा है. इन्हें मुफ्त की जमीन की चाहत रहती है जिस से मेहनत न करनी पड़े. साधुसंत भी समझने लगे हैं कि बुढ़ापे में अशक्तता के चलते भीख भी नहीं मिलनी है, इसलिए भलाई इसी में है कि बुरे वक्त के लिए पैसा व जमीनजायदाद इकट्ठी की जाए. इन की इस कमाई व गहनों को लूटने में चोर, लुटेरे और डाकू भी कोई रहम, लिहाज या रियायत नहीं करते.