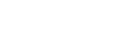लेखिका- इंदिरा दांगी
मन अच्छा हो गया. मैं ने कमर पर कसे बेटे के हाथों को नरमी से थपथपाया. उस ने जैसे मेरी देह की भाषा पढ़ ली और पटरपटर बातें करने लगा, ‘‘मम्मा, पापा का काम कितनी देर में होगा?’’
‘‘बस, थोड़ी देर में.’’
‘‘फिर हम क्या करेंगे?’’
‘‘घर चलेंगे.’’
‘‘नहीं, मम्मा, हम भारत भवन चलेंगे,’’ उस ने पूछा नहीं, बताया.
सपने सी वीआईपी सड़क खत्म हुई और अब हमें अतिव्यस्त चौराहा पार करना था. ठीक इसी समय, दाहिनी पलक फिर थरथराई और माथे की शिकन में तबदील हो गई. मैं सामने सड़क से गुजरती गाडि़यों को गौर से देखने लगी. स्कूटी बढ़ाने को होती और रुकरुक जाती. रहरह कर आत्मविश्वास टूट रहा था और मुझे लगने लगा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी, इन में से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में अचानक आ निकलेगा और हमें रौंदता चला जाएगा. मेरे पैर स्कूटी के दोनों तरफ जमीन पर टिके थे. यह मैं थी जो हमेशा कहती रही कि ड्राइविंग करते वक्त बारबार जमीन पर पैर टिकाने वाले कच्चे ड्राइवर होते हैं और उन बुजदिल लमहों में मेरा बरताव नौसिखिए स्कूटर ड्राइवरों से भी बदतर था.
कई बार मैं आगे बढ़ी, डर और परेशानी से पीछे हटी और इस तरह पता नहीं मैं कितनी देर वहां तमाशा बनी खड़ी रहती, उस मोड़ पर जिसे मैं सैकड़ों दफा पार कर चुकी थी. पर भला हो उस कार वाले का जिस ने मेरे पीछे से आते हुए सड़क पार करने का इंडीकेटर दिया. झट मैं ने अपनी दुपहिया उस बड़ी कार की ओट में कर ली और उस के समानांतर चलते हुए आखिर सड़क पार कर ली.