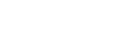पिछला भाग- फैसला दर फैसला: भाग 1
रात का भोजन समाप्त कर हम ऊपर शयनकक्ष में आ गए. बरबस ही मेरा ध्यान स्टूल पर रखे उस के बेटे के फोटो की तरफ चला गया. कुछ पूछने से पहले मैं ने उसे किसी गुरु की तरह समझाना शुरू किया, ‘‘इशि, जिंदगी उतनी सपाट नहीं है. एक बार दुखों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. उस के बाद सुखों की ढलान आती है... जब तक इन तकलीफों से
गुजरो नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम ने
कुछ किया...’’
‘‘शादीब्याह जब मसला बन जाए तो औरतमर्द के रिश्ते की अहमियत ही क्या रह जाती है? रिश्तों की आंच ही न रहे तो सांसों की गरमी एकदूसरे को जला सकती है, उन्हें गरमा नहीं सकती,’’ उस की वाणी अवरुद्ध हो गई थी.
मैं ने उस की दुखती रग को छू दिया, ‘‘कुछ कहेगी नहीं?’’
‘‘हारे हुए जुआरी की तरह सबकुछ लुटा कर खाली हाथ चली आई हूं... पूरे घर को बांधने के प्रयास में जान ही नहीं पाई कि जिस डोर से बांधने का प्रयास किया वह डोर ही कच्ची थी... जितना बांधने का प्रयास करती, उतनी ही डोर टूटती चली जाती... समझ ही नहीं पाई कि मैं गलत कहां थी?
‘‘एक बार फिर सोच लो इशिता,’’
मैं ने कहा.
‘‘आपसी बेलागपन के बावजूद मेरा नारी स्वभाव हमेशा इच्छा करता रहा सिर पर तारों सजी छत की... मेरी छत मेरा वजूद था... बेशक इस के विश्वास और स्नेह का सीमेंट जगहजगह से उखड़ रहा था. फिर भी सिर पर कुछ तो था... पर मेरे न चाहने पर भी मेरी छत मुझ से छीन ली गई... मेरा सिर नंगा हो गया. सब उजड़ गया. नीड़ का तिनकातिनका बिखर गया. प्रेम का पंछी दूर कहीं क्षितिज के पार गुम हो गया,’’ इशिता